 संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय :
संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय :
मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएँ न हों यह संभव नहीं है।
समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएँ मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिये जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है।
भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है ‘चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी‘ , इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी और झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहाँ विस्तृत और परिवर्तित हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएँ अलग हो गयी। इन दिनों सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गये हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं।
एक समय में विकसित और विकासशील देशों की बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजूद हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया, जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकि माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहाँ यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन (संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है।
विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नये प्रश्न खड़े किये हैं, जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुँची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराइयाँ हमारी पंचायतों तक नहीं पहुँच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुँच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे-धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख-दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके।
हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएँ बढ़ गयी हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गये हैं, किंतु इनसे आम-आदमी गायब है। चैनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है, जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुँच सकते, मीडिया उन तक पहुँचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएँ। जैसे बिहार का एक गाँव धौरहरा है, जहाँ बच्ची होने पर गाँव में आम का पेड़ लगाते हैं।
हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चिंताएँ अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिंताएँ कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएँ हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयँ रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब माँगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी।
(देश मंथन, 10 जून 2016)



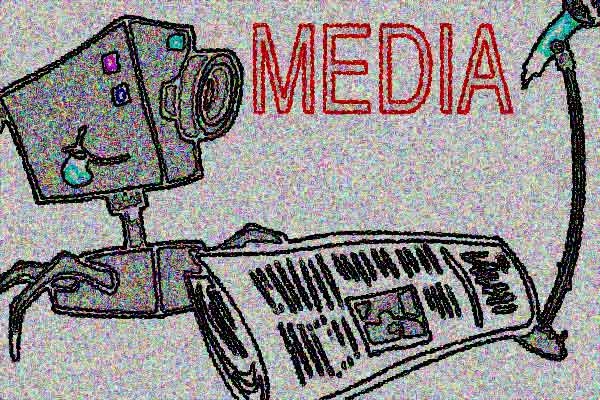
 संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय :
संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय :












